भारतीय संविधान का इतिहास और विकास – विस्तृत नोट्स एवं प्रैक्टिस सेट
भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यह सरकार, उसके संगठनों, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का ढांचा प्रदान करता है। मूल रूप में इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, जो इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाता है। इसे तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे। यह गणतांत्रिक और संघीय ढांचे वाला संविधान है, जिसमें संसदीय प्रणाली के तत्व शामिल हैं।
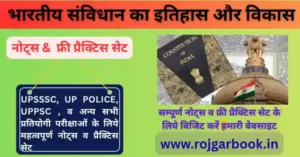
भारत की विशालता और विविधता
स्वतंत्रता के समय भारत एक विशाल और विविध देश था, जिसमें 562 रियासतें थीं। संविधान निर्माताओं ने एक विस्तृत दस्तावेज़ तैयार किया ताकि विविधता को समाहित करते हुए एकता और स्थिरता सुनिश्चित हो। भारत सरकार अधिनियम, 1935 का संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद सीधे लिए गए। यह संवैधानिक विकास का परिणाम था, जो ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुआ।
ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास
ब्रिटिश शासन ने भारत में संवैधानिक ढांचे की नींव रखी। विभिन्न अधिनियमों ने शासन प्रणाली को आकार दिया, जो भारतीय संविधान का आधार बने।
प्रमुख संवैधानिक अधिनियम
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773:
प्रावधान: ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल बनाया (वॉरेन हेस्टिंग्स पहले)। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक।
प्रभाव: केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत। कंपनी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा।
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784:
प्रावधान: कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग किए। नियंत्रण बोर्ड बनाया। द्वैध शासन शुरू। भारत को “ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र” कहा गया।
प्रभाव: ब्रिटिश सरकार का भारत पर सीधा नियंत्रण। कंपनी प्रशासनिक निकाय बनी।
चार्टर एक्ट, 1813:
प्रावधान: कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार (चाय और चीन व्यापार को छोड़कर) समाप्त। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान। मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति।
प्रभाव: मुक्त व्यापार और शिक्षा की शुरुआत।
चार्टर एक्ट, 1833:
प्रावधान: कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त। बंगाल का गवर्नर-जनरल “भारत का गवर्नर-जनरल” बना (विलियम बेंटिक पहले)। विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण। भारतीय विधि आयोग (लॉर्ड मैकाले)। दास प्रथा समाप्त।
प्रभाव: प्रशासन का केंद्रीकरण। सिविल सेवा में योग्यता आधारित नियुक्तियाँ।
भारत सरकार अधिनियम, 1858:
प्रावधान: कंपनी का शासन समाप्त। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन। भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद बनी। गवर्नर-जनरल को वायसराय कहा गया (लॉर्ड कैनिंग पहले)। चूक का सिद्धांत खत्म।
प्रभाव: प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। रियासतों के साथ संबंध मजबूत।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861:
प्रावधान: भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल किया। प्रांतीय विधान परिषदें बनीं। वायसराय को अध्यादेश का अधिकार। पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू।
प्रभाव: भारतीयों की सीमित भागीदारी। विकेंद्रीकरण की शुरुआत।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892:
प्रावधान: विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्य। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार। अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू।
प्रभाव: भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार):
प्रावधान: भारतीयों को विधायी और कार्यकारी परिषदों में शामिल किया (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले)। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल।
प्रभाव: सांप्रदायिक राजनीति की नींव। भारतीयों की भागीदारी बढ़ी।
भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार):
प्रावधान: प्रांतों में द्वैध शासन। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। प्रत्यक्ष निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार।
प्रभाव: उत्तरदायी सरकार की शुरुआत। संसदीय प्रणाली की नींव।
भारत सरकार अधिनियम, 1935:
प्रावधान: अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित। तीन सूचियाँ (संघ, प्रांतीय, समवर्ती)। प्रांतीय स्वायत्तता। संघीय न्यायालय। सीमित मताधिकार।
प्रभाव: भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत। संघीय ढांचा और स्वायत्तता की नींव।
संविधान सभा का गठन और कार्यप्रणाली
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत हुआ। यह भारत के संविधान निर्माण का आधार थी।
कैबिनेट मिशन योजना, 1946
उद्देश्य: भारत को सत्ता हस्तांतरण, एकता बनाए रखना, और संविधान सभा का गठन।
सदस्य: लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर।
प्रावधान:
संविधान सभा का गठन, जिसमें 389 सदस्य (292 प्रांतों, 93 रियासतों, 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से)।
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुनाव।
अंतरिम सरकार की स्थापना (2 सितंबर, 1946, जवाहरलाल नेहरू उप-प्रधानमंत्री)।
संघीय ढांचा: विदेश, रक्षा, संचार केंद्र के पास; बाकी प्रांतों के पास।
तीन समूह: समूह ‘क’ (हिंदू बहुल), ‘ख’ और ‘ग’ (मुस्लिम बहुल)।
रियासतें भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्र हो सकती थीं।
प्रभाव: भारत की एकता का प्रयास, लेकिन कांग्रेस-मुस्लिम लीग की असहमति से विफल। विभाजन की ओर कदम।
माउंटबेटन योजना, 1947
उद्देश्य: विभाजन और सत्ता हस्तांतरण।
प्रावधान:
भारत और पाकिस्तान में विभाजन (15 अगस्त, 1947)।
बंगाल और पंजाब का विभाजन। जनमत संग्रह (सिलहट, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत)।
रियासतों को भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्रता का विकल्प।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा।
दो संविधान सभाएँ: भारत और पाकिस्तान।
प्रभाव: विभाजन औपचारिक। सांप्रदायिक हिंसा और पलायन। भारत की संविधान सभा को नए ढांचे में काम।
अंतरिम सरकार का गठन
अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत हुआ, जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया और क्विट इंडिया आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के लिए चुनावों में भाग लिया।
गठन की प्रक्रिया
- संविधान सभा का चुनाव: अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हुए, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं ने प्रतिनिधियों का चयन किया। कांग्रेस ने 69% सीटें (208) जीतीं, जबकि मुस्लिम लीग ने 73 सीटें प्राप्त कीं।
- कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव: मिशन ने 14 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसमें 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, और 3 अल्पसंख्यक प्रतिनिधि शामिल थे। वायसराय को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
- प्रारंभिक असहमति: मुस्लिम लीग ने शुरू में सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। लीग ने 2 सितंबर, 1946 को “ब्लैक डे” के रूप में मनाया और काले झंडे फहराए।
- मुस्लिम लीग की भागीदारी: जुलाई 1946 में जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए लीग 26 अक्टूबर, 1946 को सरकार में शामिल हुई।
अंतरिम सरकार की संरचना
अंतरिम सरकार का कार्यकारी अंग वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जिसे मंत्रियों की परिषद में बदल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और वास्तविक प्रधानमंत्री थे। सरकार में शामिल प्रमुख सदस्य निम्नलिखित थे:
- वायसराय और गवर्नर-जनरल: विस्काउंट वावेल (फरवरी 1947 तक), लॉर्ड माउंटबेटन (फरवरी 1947 से)।
- जवाहरलाल नेहरू (कांग्रेस): उपाध्यक्ष, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध।
- सरदार वल्लभभाई पटेल (कांग्रेस): गृह मामले, सूचना और प्रसारण।
- राजेंद्र प्रसाद (कांग्रेस): कृषि और खाद्य।
- सी. राजगोपालाचारी (कांग्रेस): शिक्षा और कला।
- बलदेव सिंह (कांग्रेस): रक्षा।
- जगजीवन राम (कांग्रेस): श्रम।
- लियाकत अली खान (मुस्लिम लीग): वित्त (26 अक्टूबर, 1946 से)।
- अब्दुर रब निश्तार (मुस्लिम लीग): डाक और वायु।
- इब्राहिम इस्माइल चुंडरीगर (मुस्लिम लीग): वाणिज्य।
- जोगेंद्र नाथ मंडल (मुस्लिम लीग): कानून (अनुसूचित जाति हिंदू)।
- गजनफर अली खान (मुस्लिम लीग): स्वास्थ्य।
- सी.एच. भाभा (कांग्रेस): कार्य, खान और ऊर्जा।
- जॉन मथाई (कांग्रेस): उद्योग और आपूर्ति।
- असफ अली (कांग्रेस): रेलवे और परिवहन।
मुस्लिम लीग के शामिल होने के लिए तीन कांग्रेस सदस्यों (शरत चंद्र बोस, सैयद अली जहीर, और सर शफात अहमद खान) ने इस्तीफा दिया।
संविधान सभा की संरचना
गठन: नवंबर 1946 में। कुल 389 सदस्य, विभाजन के बाद 299।
पहली बैठक: 9 दिसंबर, 1946, नई दिल्ली (संविधान हॉल)।
अध्यक्ष:
अस्थायी: डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा।
स्थायी: डॉ. राजेंद्र प्रसाद (11 दिसंबर, 1946)।
संवैधानिक सलाहकार: बी.एन. राव।
प्रमुख सदस्य: जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, के.एम. मुंशी, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख।
विशेषता: सभी समुदायों, धर्मों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व।
महत्वपूर्ण समितियाँ
- प्रारूप समिति: डॉ. बी.आर. आंबेडकर (7 सदस्य: के.एम. मुंशी, गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन. माधव राव, टी.टी. रामकृष्ण चारी)।
- संघ शक्ति समिति: जवाहरलाल नेहरू।
- संघ संविधान समिति: जवाहरलाल नेहरू।
- प्रांतीय संविधान समिति: सरदार वल्लभभाई पटेल।
- मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति: सरदार वल्लभभाई पटेल।
- राष्ट्रीय ध्वज समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
- मौलिक अधिकार उप-समिति: जे.बी. कृपलानी।
- अल्पसंख्यक उप-समिति: एच.सी. मुखर्जी।
उद्देश्य प्रस्ताव
- प्रस्तुति: 13 दिसंबर, 1946, जवाहरलाल नेहरू।
- स्वीकृति: 22 जनवरी, 1947।
- मुख्य बिंदु: भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत।
- प्रभाव: संविधान का आधार बना।
संविधान निर्माण की प्रक्रिया
- समय: 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन (11 सत्र)।
- मसौदा: प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में पहला मसौदा, 4 नवंबर 1948 में अंतिम मसौदा पेश किया।
- चर्चा: तीन चरणों में। 7,635 संशोधन प्रस्ताव, 2,473 स्वीकृत।
- अंगीकरण: 26 नवंबर, 1949 (संविधान दिवस)।
- लागू: 26 जनवरी, 1950 (गणतंत्र दिवस)।
- हस्तलिखित प्रतियाँ: अंग्रेजी (प्रेम बिहारी नारायण रायजादा), हिंदी (बसंत कृष्ण वैद्य)। संसद भवन में सुरक्षित।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
सबसे लंबा लिखित संविधान:
- मूल: 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग।
- वर्तमान: ~470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग।
- कारण: भारत की विविधता, ऐतिहासिक प्रभाव (1935 अधिनियम), एकल संविधान, विधिवेत्ताओं का योगदान।
कठोरता और लचीलापन:
- साधारण बहुमत: नए राज्य, नागरिकता।
- विशेष बहुमत: मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व।
- विशेष बहुमत + आधे राज्यों की मंजूरी: संघीय ढांचा, राष्ट्रपति चुनाव।
संघीय प्रणाली:
- केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन (संघ, राज्य, समवर्ती सूची)।
- एकात्मक झुकाव: मज़बूत केंद्र।
संसदीय स्वरूप:
- राष्ट्रपति (राज्य प्रमुख), प्रधानमंत्री (सरकार प्रमुख)।
- कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी।
एकल नागरिकता:
- केवल भारतीय नागरिकता, कोई राज्य-विशिष्ट नागरिकता नहीं।
स्वतंत्र न्यायपालिका:
- सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक।
- न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 32, 226)।
धर्मनिरपेक्षता:
- 42वाँ संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में शामिल।
- सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। अनुच्छेद 25: धर्म की स्वतंत्रता।
संविधान के स्रोत
भारत सरकार अधिनियम, 1935: संघीय तंत्र, आपातकाल, लोक सेवा आयोग।
ब्रिटिश संविधान: संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता।
अमेरिकी संविधान: मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति।
आयरिश संविधान: नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति चुनाव।
कनाडाई संविधान: संघीय ढांचा, अवशिष्ट शक्तियाँ।
ऑस्ट्रेलियाई संविधान: समवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार।
फ्रांसीसी संविधान: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व।
सोवियत संविधान: सामाजिक-आर्थिक न्याय।
दक्षिण अफ्रीकी संविधान: संशोधन प्रक्रिया।
जापानी संविधान: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
भारतीय स्रोत: प्राचीन ग्रंथ, गांधीवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता संग्राम।
